Content will be available soon

















2017 में, उत्तर प्रदेश में केवल 4 हवाई अड्डे (लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा) कार्यशील थे, जो 25 स्थानों से जुड़े थे। अब प्रदेश में 15 हवाई अड्डे कार्यशील हैं, जिनमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, बरेली, कानपुर, हिंडन, कुशीनगर, अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद सम्मिलित हैं। ये हवाई अड्डे 80 से अधिक जगहों से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं तथा एक और हवाई अड्डा (जेवर, गौतम बुद्ध नगर) विकसित हो रहा है। पिछले 7 वर्षों में, राज्य सरकार ने 11 हवाई अड्डों का विकास किया है -प्रयागराज, हिंडन, बरेली, कुशीनगर, कानपुर, अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद। इसके अतिरिक्त, 3 और हवाई अड्डे (सहारनपुर, आगरा और ललितपुर) बन रहे हैं। अगले दो वर्षों में, कुल 21 हवाई अड्डे (5 अंतरराष्ट्रीय और 16 घरेलू) उत्तर प्रदेश में कार्यशील हो जायेंगे।
उत्तर प्रदेश में घरेलू यात्री ट्रैफिक वित्त वर्ष 2019-20 में 87.90 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 102.08 लाख हो गया है। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय यात्री ट्रैफिक वित्त वर्ष 2019-20 में 9.69 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 10.93 लाख हो गया है। उत्तर प्रदेश में कार्गो ट्रैफिक भी वित्त वर्ष 2019-20 में 18,615 मीट्रिक टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 25,915 मीट्रिक टन हो गया है।
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे
कम सुविधा वाले और उभरते क्षेत्रों में नए, आधुनिक हवाई अड्डों का विकास।
हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण-
बढ़ते यात्री और माल यातायात को संभालने के लिए मौजूदा हवाई अड्डे के टर्मिनलों, रनवे और सहायक अवस्थापना को उन्नत और विस्तारित करना।
कार्गो टर्मिनल
लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स और खराब होने वाले सामान के परिवहन को समर्थन देने के लिए समर्पित एयर कार्गो हब का विकास।
विमान विनिर्माण इकाइयां-
विमान घटकों को एसेंबेल करने और विनिर्माण के अवसर।
एमआरओ सुविधाएं
विमान के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना।
उत्तर प्रदेश सरकार की एयरस्ट्रिप नीति, 2023
यह नीति उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ), विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) आदि जैसी विभिन्न विमानन गतिविधियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एयरस्ट्रिप के उपयोग का अवसर प्रदान करती है।
क्षेत्रीय एयरलाइंस-
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के अंतर्गत टियर-2 और टियर-3 शहरों की सेवा के लिए क्षेत्रीय वाहक शुरू करने के अवसर।
चार्टर सेवाएं-
निजी चार्टर की मांग बढ़ रही है, विशेष रूप से व्यावसायिक यात्रा और पर्यटन के लिए।
कार्गो एयरलाइंस-
कृषि निर्यात और औद्योगिक माल परिवहन का समर्थन करने के लिए समर्पित कार्गो एयरलाइंस।
एचईएमएस
हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं
पायलट प्रशिक्षण अकादमियां-
एयरलाइन संचालन में वृद्धि के साथ प्रशिक्षित पायलटों की मांग बढ़ रही है।
तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान-
एमआरओ, ग्राउंड हैंडलिंग और हवाई यातायात नियंत्रण के लिए इंजीनियरों और तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षित करने की सुविधाएं।
ईंधन सेवाएं
विमानन ईंधन आपूर्ति, भंडारण और ईंधन भरने संबंधी अवस्थापना में निवेश।
ग्राउंड हैंडलिंग-
बैगेज हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट सर्विसिंग और कार्गो संचालन में अवसर।
आतिथ्य और खुदरा
यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एयरपोर्ट लाउंज, फूड कोर्ट और खुदरा दुकानों का विस्तार।
स्मार्ट एयरपोर्ट -
यात्री प्रसंस्करण, सुरक्षा और संचालन के लिए एलओटी, एआई और बायोमेट्रिक सिस्टम जैसी उन्नत तकनीकों में निवेश करना।
वायु यातायात प्रबंधन प्रणाली -
कुशल हवाई क्षेत्र प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए उन्नत नेविगेशन और निगरानी प्रणालियों का कार्यान्वयन।
ड्रोन प्रौद्योगिकी -
लॉजिस्टिक्स, निगरानी और कृषि के लिए मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) और संबंधित सेवाओं का विकास।
| Sr. No. | Department Name | Service Name | Timeline (Days) | Category | Criteria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
Board of Revenue | Land Purchase Permission (Dhara 89) | 60 | In case applicant wants to purchase more than 12.5 Acre Land | ||
| Change of Land Use (Section 80) | 45 | In case applicant wants to change agriculture land to non-agriculture land | ||||
 |
Department of Labor Website Link |
Approval of plan and permission to construct/extend/or take into use any building as a factory under the Factories Act, 1948 | 30 | If factory having 40 or more workers without power. Or Factory having 20 or more workers with power. | ||
| Registration and grant of license under The Factories Act, 1948 | 30 | If factory having 40 or more workers without power. Or Factory having 20 or more workers with power. | ||||
| Registration of principal employer's establishment under provision of The Contracts Labor (Regulation and Abolition) Act, 1970 | 30 | Every establishment in which 50 or more workmen are employed | ||||
| Registration of establishment under the Inter State Migrant Workmen (RE/CS) Act, 1979 | 30 | Every establishment in which 5 or more inter-state migrant workmen are employed. | ||||
| Registration under The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 | 30 | Govt - Unit any number and Pvt unit 10 and more employee and Investment 10 Lac and above any number of employees | ||||
 |
Department of Stamp and Registration Website Link |
Property Registration | 1 | If applicant wants to register properties | ||
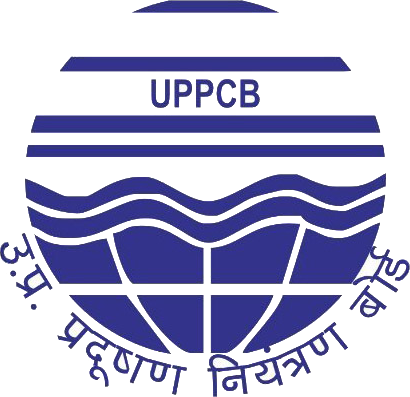 |
Pollution Control Board Website Link |
Consent to Establish Under Air and Water Act (NOC) | 120 | Mandatory | ||
| Consolidated Form for Consent under Water Act 1974 Air Act 1981 and authorization under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 | 120 | Mandatory | ||||
| Registration under Plastic Waste Management Rules 2016 | 90 | If applicant deals with plastic waste | ||||
| Authorization under E-Waste (Management) Rules 2016 | 120 | If applicant deals with e- waste | ||||
 |
Uttar Pradesh Fire Services Website Link |
NOC from Fire Department (prior to commencement of construction activities) or Provisional | 15 | Mandatory | ||
 |
Uttar Pradesh Power Corporation Limited Website Link |
Power Connection | 30 | If applicant require power connection | ||
 |
Forest and Wildlife Department Website Link |
NOC for Tree Felling | 15 | If applicant wants to cut tree | ||
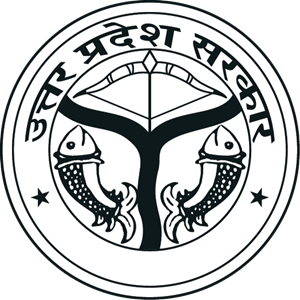 |
Registrar Firms Societies and Chits Website Link |
Registration of Partnership firms, Society | 30 | If applicant wants to register Firm or Society | ||
 |
Public Works Department Website Link |
Road Cutting Permissions | 7 | In case applicants wants cut road | ||
 |
Directorate of Electrical Safety Website Link |
Initial Inspection of Low Voltage Installation | 4 | If applicant require power connection | ||
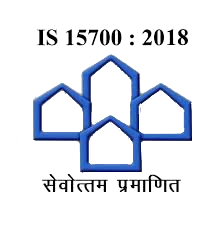 |
|
Building Plan Approval | 15 | In case applicant wants to construct building | ||
| Occupancy Certificate | 25 | In case applicant wants to obtain Occupancy Certificate | ||||
 |
Urban Department Website Link |
Water Connection of Industrial Water | 15 | In case applicant wants a water connection | ||